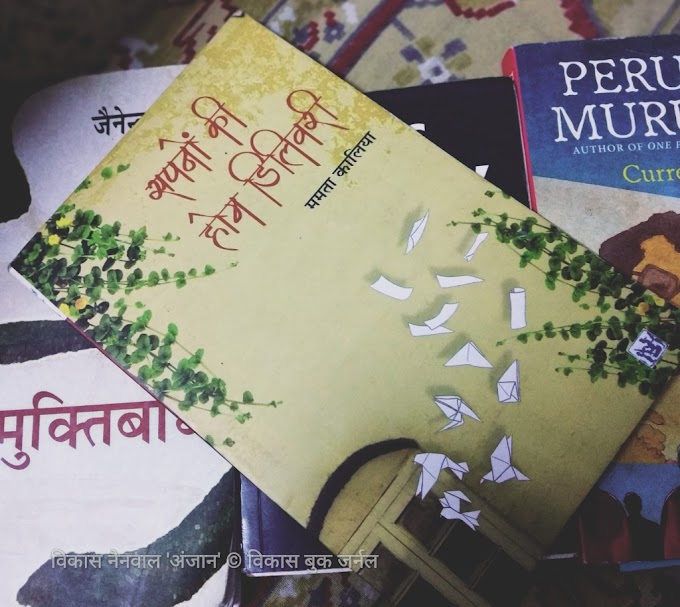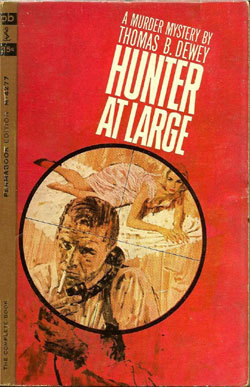लेखक सुरेन्द्र मोहन पाठक ने शृंखलाबद्ध उपन्यास लिखे हैं लेकिन उसके साथ साथ कई एकल उपन्यास भी लिखे हैं। 1982 में प्रथम बार प्रकशित हुआ 'लम्बे हाथ' भी उनका एकल उपन्यास है जिसका घटनाक्रम विशालगढ़ नामक कस्बे में घटित होता है। यह एक रहस्यकथा है जो अंत तक आपको बाँध कर रखती है।
आज एक बुक जर्नल पर हम आपके लिए सुरेन्द्र मोहन पाठक के इसी रहस्यकथा 'लम्बे हाथ' का एक रोचक अंश लेकर आ रहे हैं। उम्मीद है यह अंश आपको पसंद आएगा और पुस्तक के प्रति आपकी उत्सुकता जगाएगा।
एकाएक मेरी नींद खुल गई।
कहीं घंटी बज रही थी।
मैं नींद की खुमारी को रफा करने की कोशिश करता हुआ सोचने लगा कि घंटी कहाँ बज रही थी!
फिर मुझे सूझा कि वह कोठी की कॉलबेल नहीं, राजू की घंटी थी जो नर्स के कमरे में बजती थी।
मैं खामोश पलंग पर लेटा रहा।
आशा ने घंटी की आवाज सुन ली होगी और वह राजू के पास पहुँच गयी होगी।
लेकिन घंटी फिर बजी।
मैंने फिर भी प्रतीक्षा की।
जब तीसरी बार घंटी बजी तो मैं उठ खड़ा हुआ।
आशा घंटी सुन क्यों नहीं रही थी?
मैं अपने कमरे से निकलकर आगे बढ़ा।
मैंने आशा के कमरे का दरवाजा बंद पाया।
मैं राजू के पास पहुँचा।
“क्या बात है, बेटा?” - मैं बोला।
“मुझे प्यास लगी है।” - वह बोला - “आशा दीदी कहाँ हैं?”
“लगता है आशा को घंटी की आवाज सुनाई नहीं दी?”
“मैं तो कई बार घंटी बजा चुका हूँ। कौशल्या आंटी तो हमेशा पहली घंटी की आवाज सुन लेती हैं।”
“शायद आशा को रात की ड्यूटी देने की आदत नहीं है, बेटा। मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ।”
मैंने उसे पानी पिलाया।
“और कुछ?” - मैं बोला।
उसने इनकार में सिर हिलाया।
“अब सो जाओ।”
“अच्छा।”
“गुड नाइट।”
“गुड नाइट, डैडी।”
मैं उसके कमरे से बाहर निकला।
मैंने आशा के कमरे के दरवाजे को हौले से धक्का दिया।
दरवाजा भीतर से बंद नहीं था।
मैंने कमरे में झाँका।
कमरा खाली था।
तभी मुझे सीढ़ियों की तरफ से बहुत हल्की-सी आहट सुनाई दी।
मैंने सीढ़ियों के दहाने पर पहुँचा।
आशा दबे पाँव सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर आ रही थी।
मुझ पर निगाह पड़ते ही वह थमक कर खड़ी हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह कुछ क्षण मुँह बाये अपलक मुझे देखती रही और फिर भारी कदमों से बाकी की सीढ़ियाँ तय करके मेरे पास तक पहुँची।
“क... क्या हुआ?”- वह बोली।
“राजू की घंटी बज रही थी।” - मैं सहज भाव से बोला।
“ओह! ...मैं जरा नीचे चली गयी थी।”
“नीचे कहाँ?”
“बाहर लॉन में। मेरा दिल घबरा रहा था। मैंने सोचा था जरा ताजी हवा लगेगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी।”
“अब ठीक हो गयी हो तुम?”
“ज... जी... जी हाँ। दरअसल रात की ड्यूटी की मुझे आदत नहीं। मुझे बेचैनी महसूस होने लगी थी और यह भी डर लगने लगा था कि मैं कहाँ गहरी नींद न सो जाऊँ।”
“आई सी।”
मैंने नोट किया कि उसके बाल बड़े करीने से सजे हुए थे, चेहरे पर हल्का सा मेकअप भी था और वह ऊँची एड़ी की सैंडल पहने हुए थी।
बाहर कोठी के लॉन में ताजी हवा खाने भी वह पूरे बनाव-शृंगार के साथ गयी थी।
“ऐनी वे” - मैं बोला- “गुड नाइट।”
“ग... गुड नाइट।”- वह बोली।
मैं अपने कमरे में आ गया।
मैंने घड़ी पर निगाह डाली।
पौने दो बजे थे।
मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया और उसके कश लगाता हुआ सोचने लगा।
कहीं कोई गड़बड़ थी।
आशा अगर लॉन में टहलने ही गयी थी तो वह इतनी घबरायी हुई क्यों थी? मुझे देखते ही उसके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया था?
मैंने सिगरेट ऐश-ट्रे में झोंक दिया और दबे पाँव अपने कमरे से बाहर निकला। बिना कोई बत्ती जलाए मैं सीढ़ियाँ उतरकर नीचे पहुँचा। सावधानी से, बिना आवाज किए, कोठी का मुख्य द्वारा खोलकर मैं बाहर निकल आया।
पोर्टिको में मेरी कार के आगे मुक्ता की कार खड़ी थी। मैं उसके समीप पहुँचा। मैंने उसके हुड पर हाथ रखा।
हुड गर्म था।
यानी की मुक्ता की कार हाल ही में इस्तेमाल की गयी थी।
कोई अंधा भी यह नतीजा निकाल सकता था कि इतनी रात गए आशा मुक्ता की कार पर कहीं गयी थी।
मैंने वापस अपने कमरे में आ गया।
बाकी की रात मैंने बड़ी बेचैनी से काटी।
आठ बजे मैं सोकर उठा तो मैंने आशा को तब भी ड्यूटी पर पाया।
“मैंने कौशल्या से फिर ड्यूटी बदल ली है।” - उसने बिना माँगे सफाई पेश की - “रात की शिफ्ट की ड्यूटी मुझे रास नहीं आयी।”
“मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता था।” - मैं बोला।
“बात?”
“हाँ।”
“कौन-सी बात?”
“कल रात तुम कहाँ गयी थीं?”
“कल रात मैं कहाँ गयी थी?” - उसने दोहराया।
“यह तुमने मेरे सवाल का जवाब दिया है या मुझसे सवाल पूछा है?”
“मैं तो कहीं भी नहीं गयी थी।”
“कहीं तो तुम जरूर गयी थी।”
“मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरी तबियत घबरा रही थी, इसलिए मैं बाहर लॉन में टहलने चली गयी थी।”
“ऊँची एड़ी की सैंडल पहनकर?”- मैं व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला - “मुकम्मल बनाव-शृंगार करके?”
वह खामोश रही।
”तुम मुक्ता की कार पर कहाँ गयी थीं?”- मैं सख्ती से बोला।
“कार तो मुझे चलानी भी नहीं आती, मिस्टर गुप्ता।”
मैं खामोश हो गया। और क्या करता? मेरी पेश जो नहीं चल रही थी।
“आप और कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे?”- वह बोली।
“कुछ पूछना नहीं”-मैं बोला- ”कुछ कहना चाहता हूँ।”
“क्या?”
“झूठ बोलने में जैसी महारत तुम्हें हासिल है, वैसी शायद ही दुनिया में किसी को हो।”
उसको चेहरा कानों तक लाल हो गया।
“मिस्टर गुप्ता!” - यह तीव्र विरोधपूर्ण स्वर में बोली।
“हाँ।”
उसने बोलने के लिए मुँह खोला लेकिन फिर एकाएक अपने होंठ भींच लिए।
“कुछ नहीं।”- वह बोली।
फिर वह घूमी और मुझे वहीं खड़ा छोड़कर अपने कमरे में घुस गयी।
मैं ड्रॉइंग रूम में पहुँचा।
मैंने डॉक्टर रोहतगी को फोन किया।
वह लाइन पर आया तो मैंने उसे अपना परिचय दिया और उससे आशा के बारे में सवाल किया।
“आशा!”- वह बोला - “आशा माथुर। वह नर्स जो आपके बच्चे की देखभाल कर रही है?”
“जी हाँ।”
“उसे मैंने नहीं भिजवाया था, मिस्टर गुप्ता। न ही वह मेरी सिफारिश पर रखी गयी थी।”
“तो?”
“मुक्ता ने खुद ही रखा था उसे। किसी अपने वाकिफकार की सिफारिश पर।”
“वह क्वालीफाइड नर्स तो है न?”
“मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुक्ता ने उसकी क्वालीफिकेशन की बाबत तसल्ली करके ही रखा होगा उसे।”
“आपको मालूम है मुक्ता ने अपने कौन-से वाकिफकार की सिफारिश पर आशा को रखा था?”
“हाँ। सत्यनारायण ने सिफारिश की थी आशा की।”
“ओह!”
“कोई घपला है, मिस्टर गुप्ता।”
“जी नहीं। मैं यूँ ही पूछ रहा था। बहुत-बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब।”
मैंने लाइन काट दी।
तो सत्यनारायण ने आशा को वह नौकरी दिलाई थी।
मैंने सत्यनारयाण से आशा के बारे में बात करने का फैसला कर लिया।
मैं नहा-धोकर तैयार हुआ और कमर्शियल स्ट्रीट पहुँचा।
तब तक दस बज चुके थे।
मैं सोच ही रहा था कि सत्यनारायण शायद अभी तक ‘ब्लैकबर्ड’ में न पहुँचा हो कि मुझे वहाँ के पिछवाड़े की तरफ कंपाउंड के कोने में उसकी कार खड़ी दिखाई दी। मैंने भी अपनी कार सामने खड़ी करने के स्थान पर उसे पिछवाड़े की तरफ बढ़ा दिया।
कार पार्क करके मैं इमारत के पिछले दरवाजे पर पहुँचा।
मैंने सत्यनारयाण के ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक दी।
कोई उत्तर न मिला।
मैंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो उसे ताला लगा पाया।
लेकिन अगर उसकी कार वहाँ थी तो उसका वहाँ होना जरूरी था।
मैंने हॉल में पहुँचा।
हॉल खाली पड़ा था।
केवल वहाँ के कुछ कर्मचारी वहाँ की सफाई में लगे दिखायी दे रहे थे।
“बार, ग्यारह बजे खुलता है, साहब।” - मुझे देखकर उनमें से एक बोला।
“मैं सत्यनारायाण साहब को देख रहा था।”- मैं बोला।
“अगर वे यहाँ होंगे तो अपने ऑफिस में होंगे, साहब।”
“ऑफिस पर तो ताला लगा हुआ है।”
“तो फिर साहब यहाँ नहीं होंगे।”
“लेकिन उनकी कार तो बाहर खड़ी है।”
“तो फिर वे यहीं होंगे।”
“यहाँ कहाँ?”
“ऑफिस में।”
“अरे, मैं कह रहा हूँ ऑफिस में ताला लगा हुआ है।”
वह कर्मचारी उलझनपूर्ण भाव से कान खुजाने लगा।
“आज सुबह से तुममें से किसी ने साहब को देखा है?”
सबने इनकार में गर्दन हिलायी।
“ऑफिस की चाबी कौन रखता है?”
“साहब रखते हैं।”
“और कौन रखता है?”
“बारटेंडर। लेकिन अभी वह आया नहीं है। वह ग्यारह बजे आएगा।”
“यह पक्की बात है कि साहब इमारत में और कहीं नहीं है?”
“जी हाँ।”
मैं वहाँ से हटा है और फिर उसके ऑफिस के दरवाजे पर पहुँचा।
दरवाजा न केवल बंद था, वैसे ताले से बंद था जो कुंडे में पिरोकर लगाया जाता है। दरवाजे में स्प्रिंग लॉक होता तो मैं सोच सकता था कि शायद सत्यनारायण भीतर से ताला बंद करके बैठा हुआ हो।
लेकिन अगर वह वहाँ नहीं था तो उसकी कार वहाँ क्यों थी? मुझे एक ही जवाब सूझा।
पिछली रात कार शायद एकाएक बिगड़ गई थी और उसे कार को मजबूरन वहाँ छोड़कर जाना पड़ा था। पिछली रात मुक्ता के दाह-संस्कार के बाद जब वह शमशान घाट से क्लब के लिए रवाना हो रहा था तो मैंने उसकी कार को स्टार्टिंग ट्रबल देते देखा था।
या फिर वह सुबह कार पर यहाँ आया था और उसे यहाँ खड़ी छोड़कर बिना इमारत के भीतर कदम रखे अगल-बगल कहीं चला गया था।
मैं अपनी कार के समीप पहुँचा।
मेरी निगाह एक बार फिर सत्यनारायण की कार की तरफ उठ गयी।
उसका अगला एक दरवाजा मुझे थोड़ा-सा खुला हुआ लगा।
उसे बंद कर देने की नीयत से मैं कार के समीप पहुँचा तो मेरी निगाह कार के भीतर भी पड़ी।
अगली सीट पर एक पहलू के बल गुच्छा-मुच्छा सा हुआ एक मानव शरीर पड़ा था।
मैंने घबराकर कार का दरवाजा खोला और भीतर झाँका।
वह सत्यनारायण था।
उसके कपड़े खून से तर थे। उसकी पीठ में कंधे के नीचे एक सुराख दिखाई दे रहा था जिसके इर्द-गिर्द खून बह-बहकर जम गया था।
मैंने उसकी नब्ज टटोली।
वह मर चुका था।
उसका जिस्म अकड़ना शुरू हो भी चुका था।
पता नहीं वह कब का मरा पड़ा था।
*****
पुस्तक विवरण:
फॉर्मैट: ई-बुक | प्रकाशक: डेलीहंट | प्रथम प्रकाशन: 1982
यह भी पढ़ें
- जयदीप शेखर द्वारा अनूदित बिभूतिभूषण बंद्योपाध्याय के उपन्यास 'चाँद का पहाड़' का एक रोचक अंश
- राजभारती के इन्द्रजीत शृंखला के उपन्यास 'परायी आग' का एक रोचक अंश
- अनिल मोहन के उपन्यास 'आतंक का पहाड़' का एक रोचक अंश
- संतोष पाठक के उपन्यास 'मौत की दस्तक' का एक रोचक अंश
- जितेंद्र माथुर के उपन्यास 'कत्ल की आदत' का रोचक अंश