परिचय:
रुपाली नागर 'संझा' जी खंडवा मध्य प्रदेश से आती हैं। इनकी शुरूआती पढ़ाई खंडवा में ही हुई। फिर इंदौर से माध्यमिक और हायर सेकंड्री के अलावा स्नातक भी किया। उज्जैन के माधव कॉलेज से भूगोल में मास्टर्स करते हुए उन्होंने यूनिवर्सिटी टॉप किया। अट्ठारह वर्ष तक अलग अलग शहरों में अध्यापन करने के पश्चात अपने परिवार को समय देने के खातिर उन्होंने फिलहाल नौकरी से ब्रेक ले लिया है।
बकौल उनके, उनके जीवन में लोग कम और शहर ज्यादा आये हैं। कई शहरों से होने के बाद आजकल वह अपने परिवार के साथ भारत की सांस्कृतिक राजधानी कलकत्ता में निवास कर रही हैं।
कलकत्ता में रहते हुए वह परिवार, घुमक्कड़ी, लेखन और पठन-पाठन को अपना पूरा वक्त देती हैं।
रुपाली जी की निम्न किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं:
(किताबों को ऊपर दिए लिंक्स पर जाकर खरीदा जा सकता है)
रुपाली जी से निम्न माध्यमो से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है:
एक बुक जर्नल की साक्षात्कार श्रृंखला में इस बार हम आपके समक्ष रुपाली नागर 'संझा' जी से हुई बातचीत लेकर आये हैं। रुपाली जी की तीन पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इस बातचीत में हमने उनके जीवन और उनके लेखन से जुड़े पहलुओं को छूने की कोशिश की है। उम्मीद है यह बातचीत आपको पसंद आयेगी।
प्रश्न: रुपाली जी पाठकों को अपने विषय में बताये। आप कौन से शहर से है?शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? फिलहाल किधर रह रहीं हैं?
उत्तर: "मसरूफ़ है आप बहुत औ' फ़ारिग़ हम भी नहीं,
बातें हैं कई लेकिन, बात ही होती नहीं।"
आज के इस मौज़ू दौर को बेताल की तरह काँधे पर लादे हुए मेरा ये कहन अधिकतर ज़िंदगियों को विक्रमादित्य की तरह भरमाये जा रहा है। वहाँ, ठहरकर मुझसे बात करने की आपकी इस चाहना के लिए पहले-पहल तो आपका बहुत शुक्रिया।
आपके पहले सवाल का जवाब देना ही मेरे लिए बहुत दुरुह हो गया है। अपने बारे में क्या कहूँ कि कहने लायक है भी क्या? वैसे भी आत्ममोह कब अपने बारे में निष्कपट रह पाता है। मेरी ये दिली तमन्ना रही है कि मेरे व्यक्तित्व के पहलू दूसरों के नज़रिये से सामने आएँ तो उनमें मेरे व्यक्तित्व के बहुआयाम निकल सकते हैं, वो जो अमूमन स्वयं को दृष्टिगोचर नहीं होते। हालांकि वो भी पूर्णतः सच ही हो, वैसा भी होगा नहीं, क्यूँकि उसमें भी व्यक्तिगत राग द्वेष समाहित होंगें ही! तब भी।
हाँ, कुछ आधारभूत जानकारियाँ ज़रूर साझा की जा सकती हैं। जैसे
मेरे जीवनकाल की आधी सदी मेरी अपनी बनाई दुनिया के इर्द-गिर्द ही मंडराती रही है। जिसमें मेरे कुछेक जिगरी लोग शामिल रहे। चुनिंदा वे मनपसंद लोग, जो अध्ययन-अध्यापन और कला क्षेत्र से जुड़े थे। क्यूँकि मेरा दखल भी इनमें बहुत ज़्यादा था। इनके अलावा कुछ अज़ीज़ दोस्त थे। उनसे ज्यादा सैकड़ों मुझे चाहने वाले वो विद्यार्थी, जिन्हें सिखाते हुए और उनसे बहुत कुछ सीखते हुए मैंने अट्ठारह साल गुज़ारे। जीवन एक निर्बाध गति से कल-कल कर पूरे वेग से बह रहा था!
अपने उस खोल से कछुए की तरह गरदन बाहर निकाले हुए तो मुझे दो साल ही हुए हैं! तब जब मैंनें अपनी पहली किताब के सेतु के सहारे अपनी नितांत निजी दुनिया से उस दूसरी अनजान आभासी दुनिया से राब्ता जोड़ा और उस अपरिचय की वैतरणी को पार करने की कोशिश की।
मेरी पैदाइश खंडवा शहर में हुई। प्राथमिक शिक्षा यहीं हुई। फिर यहाँ से हम पापा के तबादले के चलते बाहर निकल गये! इतनी कम उमर में ही मैंनें अपना कुछ छूट जाने का दंश पाया। बिछड़ी हुई बचपन की वो सबसे मासूम और ख़ुशगवार यादें आज तलक मन की खूँटी पर ज्यूँ की त्यूँ टँगी है। पापा सरकारी महकमे में थे तो हर दो-तीन साल में तबादला हो जाता था! उनके साथ हम भी नये शहर को अपना बनाने चल पड़ते थे। धीरे-धीरे इस सबमें मज़ा आने लगा था। नया शहर, नया माहौल, नये लोग, नये मित्र पाने की उमंग से लालायित होकर मैं दो साल किसी शहर में पूरे होते ही, तबादले की मन्नत मांगते हुए उसके पूरे होने की राह तकती रहती थी।
इंदौर, धार में क्रमशः माध्यमिक और हायर सेकंडरी की पढ़ाई हुई! इंदौर से स्नातक और उज्जैन के माधव काॅलेज से भूगोल में मास्टर्स किया, और युनिवर्सिटी टाॅपर रही। इस आधार पर इसी काॅलेज में यू जी सी द्वारा सहायक प्राध्यापक के पद पर प्रथम नियुक्ति हुई। तीन साल यहाँ अध्यापन के बाद सरकारी तौर पर शिक्षा विभाग में प्रविष्टि हुई फिर ये सिलसिला चल पड़ा और अठारह साल बख़ूबी चला। झाबुआ, रतलाम, इंदौर, भोपाल कई शहर इस जद में आये। थोड़ा बाद में चलके एक वक्त ऐसा आया जब अपना देने लायक समय मैंनें अपने कैरियर से ज़्यादा अपने परिवार को देने के ख़ातिर नौकरी छोड़ दी। अब अपने हमसफर के साथ मेरी ज़िंदगी महानगर दर महानगर फर्राटे भरने लगी। वहाँ से विदेशों की ओर रुख़ हुआ। हाल फ़िलहाल सिटी ऑफ जाॅय कलकत्ता का आनंद उठा रही हूँ।
लब्बोलुआब ये कि अब मेरी दुनिया में लोग कम शहर ज़्यादा हो गये हैं। मेरा इश्क़ उनके लिए बढ़ता ही चला गया है। उनके पहलू में रहना ही मुझे भाने लगा है। उनका मोह मुझे बाँधता है।
एक हाथ में किताब और दूसरे में किसी भी शहर की उंगली थामे मैं अपना अधिकांश समय बिताती रहती हूँ।
इसी के चलते ही शायद मैं ये कह सकी कि-
"अच्छा ना होता, अगर किसी एक ही शहर में बसी रहती मैं…
पर चलो अच्छा ही हुआ, कई शहर आकर बस गये मुझ में !!"
प्रश्न: रचनाकारों के उपनाम के पीछे अक्सर रोचक कहानी रहती है?अगर आपको ऐतराज न हो तो क्या आप 'संझा' के पीछे की कहानी साझा करना चाहेंगी?
उत्तर: ऐतराज? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि ये तो मैं ख़ूब रस लेकर बताना चाहूँगी।
मूलतः इसके दो कारण हैं।
पहला ये कि मैं उन ख़ुशकिस्मत बच्चों में से हूँ जिनका बचपन अपनी दादी के सानिध्य में बीता। खंडवा में हमारा पुश्तैनी घर था। बड़े से बगीचे, आँगन, ओटले, छज्जे, सहन,चाँदनी और कई कमरों वाला। दिन भर काम में लगी रहने वाली मेरी दादी हर साँझ, घर भर में मेरी उछलकूद को या फ़िर किताबों के साथ मेरी गठजोड़ता को ज़बरदस्ती थोड़ी देर के लिए तिलांजलि दिलवाती थीं ये कह कर कि "सई-संझा की बखत काई नायी करनूँ चाइजे।बस शांत बठनूँ चाइजे। चाल आईजा तुख कहाणी सुणावुँ।"
(शाम के समय कुछ नहीं करना चाहिए। शांत मन रहना चाहिए। आओ तुम्हें कहानी सुनाऊँ)
और मैं साँझ की इस वेला खेलों, किताबों के अपने संसार से बाहर निकल उनकी गोद में समा जाती थी। खंडवा से बाहर जाते ही दो साल के भीतर वे तो चल बसी पर उनका ये वाक्य अनहद नाद की तरह मेरे भीतर बस कर निरंतर बजता रहा है। मैनें इस बात का मर्म हालांकि थोड़े बड़े होने पर जाना कि सँझा की वेला वो समय है जब सबसे पृथक हो, अपने आप के साथ एकांत में रहना चाहिए। इस धुंधलके से थोड़ी उजास छाँट लेने के लिए। ये ही वे कहती रहती थीं, जो उस बचपने में खाली उनके कहे शब्द थे, जिसकी थाप पर मैं यूँ ही डोलती रहती थी। पर बड़े होकर मैंनें उसे पारंगत नृतक की तरह साध लिया।
जो भी याद रखने लायक है, उसे किसी कीमत मैं भूलती नहीं, और जो भूल जाने जैसा है वो भूलकर भी मुझे याद आता नहीं। यही कारण है कि अपनी दादी की याद को हमेशा जीवंत रखने के लिए मैंनें उनकी 'सँझा' को अपने में आत्मसात कर लिया।आज भी हर साँझ में, ये 'सँझा' समाहित हो जाती है सब कुछ बिसराकर।
दूसरे हमारे यहाँ पितृपक्ष के पखवाड़े में सँझा नाम की लोकदेवी का लोकपर्व कुमारी कन्याएँ बड़े उत्साह से मनाती थी। दीवार पर गोबर से मांडने मानकर फूल पत्तों और रंगीन चमकीली पन्नियों से उसे सजाया जाता था। हर साँझ सब सखियाँ एक दूसरे के घर जाती, लोकगीत गाती और सँझा को अपने मन की टेक सुनाती। आख़िर में प्रसाद खुटवाती। ये शामें इतनी सरस सुंदर और उद्वेगपूर्ण रहती थी कि साल भर इस पखवाड़े प्रतिक्षा रहती थी मुझे। उसके मोह से बँधी हुई थी मैं। खंडवा छूटा तो ये सँझा भी हाथ से छूट गई। सँझा के उस आनंद रस को अपने से एकाकार कर अपने नाम में मधुर रस भरना भी इस तख़ल्लुस को अपनाने का एक कारण रहा।
तो ये थी 'सँझा' के नेपथ्य की कहानी। अपने मन के रंगों से मनचाहे चित्र गढ़ने में माहिर रही है ये सँझा।
प्रश्न: साहित्य में रूचि कब जागृत हुई? कौन से लेखक हैं जिन्होंने आपको साहित्य की तरफ़ आकर्षित किया?
उत्तर: अगर मैं कहूँ इसका बीज बचपन से पड़ा तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी।
नंदन, चंपक, पराग, कॉमिक्स, अमर चित्र कथाओं से शुरू कर कक्षा चौथी तक आते-आते ही ऊपर उठ कर कादम्बिनी, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, हंस तक जा पहुँची थी मैं। पाँचवी कक्षा में मुझे मेरे पापा ने वृहद रामचरित मानस हिंदी अनुवाद सहित पढ़ने को दी थी। मैंनें एक हफ़्ते में पूरी पढ़ ली थी। गदगद होकर एक सौ एक रुपये मुझे पुरस्कार स्वरूप दिये थे पापा ने। वो भी पहले हर कांड के नाम और उसमें से सबसे ज्यादा पसंद आने वाली घटनाओं के बारे में विस्तृत रुप से बाकायदा पूछताछ कर। तब तो उत्साह के अतिरेक में सब ललककर बता दिया था। पर बाद में ही समझ पाई थी कि ये एक तरह से ये मेरी दो बातोंं की परीक्षा थी कि मैंनें गहनता से पढ़ा और गुना कि नहीं और ये कि क्या मैं इतनी सी उमर में इतनी तेज गति से पढ़ सकने में सक्षम थी? दोनों में ही मैं खरी उतरी थी। मैं शायद इस गुण की महत्ता तब नहीं समझ पाई होऊंगी पर पापा आज भी इसके लिए फ़ख्र करते हैं। यहाँ से साहित्य की ओर झुकाव हुआ।
उस जमाने में हर दिन कहाँ से ला सकते थे किताबें ? तो माँ ने पढ़ने की ललक देखकर एक सिंधी अंकल की लाइब्रेरी से किताबें, मैगजीन किराये पर लेकर पढ़ने की आदत डलवा दी। शरतचंद्र, प्रेमचंद, टैगोर, शिवानी जैसे लोकप्रिय लेखकों की किताबें और हंस, कादम्बिनी, धर्मयुग जैसी पत्रिकाओं से साहित्य का जुड़ाव होता गया। हर दिन मैं ख़ुद माँ के साथ जाकर एक किताब लाती उसे भी एक घंटे में चाट जाती थी।
मैं कितनी ख़ुशनसीब रही कि मेरी शुरुआत ही इतनी ऊँचाई से रही।
मेरे बढ़ते चस्के को देख पापा ने माणिक वाचनालय में ले जाना शुरू किया। वहाँ से स्तरीय किताबें पढ़ने को मिली। फिर तो जो गति और धार पकड़ी तो आज तलक टूटी नहीं। लगभग पूरी की पूरी लाइब्रेरी मैं चट कर जाती थी। समझ में कितना आता था वो अलग बात थी। हर दिन की एक किताब मेरी खुराक बन गई थी। हर बार किताब लौटाते वक्त मुझ छोटी सी बच्ची से ढेरों सवाल किये जाते थे उस किताब की बाबत। मेरे पढ़ने की सच्चाई पर सवालिया निशान लगाकर। पूरे आत्मविश्वास से मैं ज़वाब भी दे देती थी। धार और रतलाम की लाएब्रेरी भी मैंनें ऐसी ही गड़प कर ली थी।
शेक्सपियर, ऑस्कर वाइल्ड, विक्टर ह्यूगो, एच जी वेल्स, ऑर्थर माॅरीसन, मोपासां, सात्र, हरमन हैज़, काफ्का, अल्बेयर कामू, स्टीफन ज़्वीग, चापेक, ओ हेनरी, गोर्की, चेखव, तुर्गनेव, दोस्तोयेवस्की, टाॅलस्टाॅय, पुश्किन, निकोलाई गोगोल, मास्त्रेसा, जैक लंडन, पर्ल एस बक, हैमिंग्वे, जाॅय विलियम्स, रुडयार्ड किपलिंग, कोनार, शेखसादी, खलील जिब्रान, शरतचंद्र, प्रेमचंद, विमल मित्र, टैगोर, गाँधी, नेहरू, निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, हरिशंकर परसाई, रेणु, पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, अमृतलाल नागर, मंटो, चुगताई, राजेन्द्र सिंह बेदी, तकषि शिवशंकर पिल्लई, धूमकेतू, नरेश मेहता, आर के नारायण, आशापूर्णादेवी, शिवानी, मन्नु भंडारी, तस्लीमा नसरीन, अमृता प्रीतम, कृष्णा सोबती, मोहन राकेश, मुक्तिबोध, कबीर, रहीम, गालिब, मीर तकी मीर, भगवती चरण वर्मा, शिवाजी सावंत, आचार्य चतुरसेन, रांगेय राघव, विष्णु प्रभाकर, नरेंद्र कोहली, रामकुमार भ्रमर, ग्राहम ग्रीन, अज्ञेय, यशपाल, मुराकामी, दुश्यंत कुमार सिलसिला चल निकला था। अब थमने का नाम नहीं ले सकता था।
ये तो कुछ नाम है जो अभी लिखते वक्त याद आ रहे। कितने मनपसंद नाम छूटकर मुझे आँखें तरेरेंगें मैं बता नहीं सकती। मैं सच में उन सबकी बड़ी गुनहगार रहूँगी। घंटों खपा दूँ फिर भी इस गुनाह की ग्लानि से उबर नहीं पाऊंगीं। ये सब थोड़े-थोड़े मुझमें हैं। मैं सबमें थोड़ी-थोड़ी भर गई हूँ।
ऐसे कई वटवृक्षों की छाँव मेरे सिर पर है।
मैं किताबों की लतखोर हो गई हूँ। एक भी दिन कोई एक किताब ख़त्म किये बिना मुझे नींद नहीं आती। हर दिन खरीद पाना भी संभव नहीं इसलिए हर किताब उठाकर दोबारा तिबारा भी गटकी है। मृत्युंजय तो मुझे इतनी पसंद कि उसे मैं एक सौ बत्तीस बार पढ़ चुकी हूँ।
फिर भी मैं कहूँगीं कि मुझ पर गहरा असर ओ हेनरी, चेखव, दोस्तोयेवस्की, शिवाजी सावंत, निर्मल वर्मा और कबीर का पड़ा है।
प्रश्न: लेखन कब शुरू हुआ? वह कौन सी चीज़ है जो लेखन के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है?
उत्तर: दर हक़ीक़त उन चिट्ठियों को हकदार मानना चाहिए जो मैं अपनी किशोरावस्था में अपने दोस्तों और कज़िन्स को लिखा करती थी। वे सबको बेहद पसंद आती थी। हर किसी की चाहत होती थी कि कम-अस-कम एक बार उसके नाम भी मेरी चिट्ठी पहुँच जाये। उनकी वो ख़्वाहिशें, वो तारीफ़े मुझे चिहुँका देती थी। मैं हर दिन की दर से चिट्ठी लिखा करती थी भले ही उसे पोस्ट बाॅक्स में ना डालूँ। या उन्हें हाथों-हाथ दे दूँ।
या मेरी डायरियों को जिसमें मैं अपने रचे मायावी मायाजाल को सारे पन्नों पर ओढ़नी की तरहा छितरा देती थी।और टांक देती थी उनमें ढेर सारी छोटी-छोटी कविताएँ, सलमा सितारों की तरह। तब भी मन नहीं भरता था तो उकेर देती थी किनारों पर कई सारे किस्सों के गोटे भी। पर वो सब अपनों के लिए था सारे संसार के लिए नहीं।
विधिवत लेखन के रुप में लिखा तो दो साल पहले ही। वो ही किताब के रुप में छप कर पहली बार अपनी सीमा रेखा लाँघकर बाहर आया। 'ऑनलाइन डेटिंग अप्राॅक्स 25:35' उपन्यास के रुप में। हालाँकि प्रकाशित होना पहले, मेरे काव्य संग्रह 'इस पार मैं' को था। किंतु प्रकाशक के विशेष अनुरोध और व्यवसायिक दृष्टि कोण के मुताबिक सामयिक रुझान के चलते ये उपन्यास पहले लाया गया बाजार में।
मेरे हिसाब से उत्प्रेरक कोई एक वज़ह नहीं होती। ख़ासतौर से जब मैं अपने संदर्भ में कह रही हूँ।
कई कारक समय-समय पर अपना सिर उठाते हैं और मैं यथासंभव उनका मान रख, उन्हें कागज के पाटले पर प्रेम पूर्वक आसीन कर देने की कोशिश करती हूँ।
कभी आसपास की उथल-पुथल का भारी बोझ अपने काँधों पर लादकर चलना मुहाल हो जाता है तो धीरे से उन्हें उतारकर पन्नों पर बिठा देती हूँ।
कभी अपने एकांत के गहरे तल में डुबकी मारकर कोई कविता सी सीप पा जाती हूँ। उसे ही शौक से सजा देती हूँ।
कभी पुरानी यादों का एलबम इतना फड़फड़ाने लगता है कि उसकी उस आवाज से निजात पाने को एक तस्वीर उसमें से निकाल कर किस्से के रुप में कागज पर चस्पा कर देती हूँ।
यात्राओं में इतनी खचाखच भरी हुई होती हूँ कि उन सुदूरवर्ती जगहों के आईने की चकाचौंध से एक तीखी चिलक सामने वाले की आँख में चिलका देती हूँ। और उसके आँखें झपझपाने पर ख़ुश हो लेती हूँ।
पर मुझे लगता है मैं आसपास घटित हो रही मानवीय प्रवृत्तियों पर गहरे नज़र रख कर उनका आकलन प्राकृतिक घटनाओं के संदर्भ में बहुत बेहतर ढंग से करने का माद्दा रखती हूँ। यहीं मुझे सबसे ज़्यादा उकसाता है, उन्हें कलमबद्ध कर देने के लिए।
प्रश्न: आपका उपन्यास ऑनलाइन डेटिंग अप्राॅक्स 25:35 जैसे नाम से लगता है ऑनलाइन डेटिंग की दुनिया के विषय में है? यहाँ जैसा दिखता है वैसा अक्सर होता नहीं है।आप इस दुनिया को कैसे देखती हैं?किताब का विचार इसी से आया?
उत्तर: हाँ, यही इसकी विषयवस्तु है। अपने आस-पास के हर युवाओं को इसमें मग्न देख कर ही इस विचार ने मूर्त रुप लिया।
आज रुबरु मिलकर बतियाने का वक्त किसी के पास नहीं हैं, काम कौड़ी का नहीं फुरसत धेले की नहीं की तर्ज़ पर। लोगों ने व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे से दूरियाँ बना ली हैं। अब वे सब इन तकनीकी माध्यमों से ही जुड़ाव महसूस करते हैं। इनके सहारे वास्तविकता से कोसों दूर आभासी दुनिया में किसी भी जगह के किसी भी कोने में बैठे दो अनजान लोग आपस में जुड़कर बातें करके अपना दिल बहला सकते हैं। कोई नहीं जानता दूसरी ओर कौन है? कैसा है? 'बस है' इतना होना काफ़ी है।
चूँकि चैट मुफ़्त है तो बातों का माध्यम भी इस उपन्यास में वही बना है। जल्दी-जल्दी टाइप करने की कोशिश कि बातों का सिरा छूट ना जाये, अगला ऊबकर चला ना जाए इसलिए वाक्य भी अत्यंत संक्षिप्त और कूट भाषा में प्रयुक्त होते हैं। चूँकि बड़े शहरों के पात्र हैं तो वहाँ की आमफ़हम अंग्रेजी मिश्रित हिंदी भाषा ज्यूँ की त्यूँ प्रवाह बनाये हुए है।
ऊपरी तौर पर रुमानियत से लदी ये कहानी हल्के-फुल्के मजाकिया ढंग से मौज-मस्ती करती हुई बतकही पर टिकी लगती है। लेकिन उस बातचीत से जो गुत्थियाँ खुल कर सामने आती हैं, वे ज़्यादा अहम है।
ये किरदार किस ढंग से बातें करते हैं? किस स्तर पर जाकर अपना दिल बहलाते हैं? कोई किसी की हकीकत जानता नहीं, या सच झूठ जो बताया जाता है, उसके आधार पर आपस में मन खोले जाते हैं। उनमें बहुतेरा उथलापन, कैसा तो झूठ भरा होता है। क्यूँकि आमने-सामने की मुलाकात जैसे, भाव भंगिमाओं और हाव भाव से सच ताड़ जाने का, कुछ बिगड़ने का भय नहीं रहता। इस आड़ में बेधड़क दमित इच्छाओं की पूर्ति की भी कोशिश होती रहती है। मन चूँकि नहीं जुड़ते, मन बहलाने की इच्छाएँ जुड़ती हैं तो जल्दी ही मन भर जाने पर छुटकारा पा जाने की उद्विग्नता भी हावी हो जाती है।
अगर दोनों पक्ष एकतार से जुड़े हैं तो गपशप लंबी चलती रहती हैं, अगरचे कोई एक दूसरे के स्तर तक नहीं पहुँच पाता तो धीरे से कन्नी काटकर दूसरी राह निकल जाता है। फिर कहीं और ये सिलसिला चल पड़ता है।
यही सब आज का सच है जो इस उपन्यास के माध्यम से सामने आया है। इससे मुँह नहीं मोड़ा जा सकता।
देर-सवेर लोग इसके निहितार्थ को समझेंगें और ये उपन्यास आज के दौर का दर्पण साबित होगा।
आपको हैरानी होगी कि कुछेक लोगों को इससे मायूसी रही कि इसमें तो सतही बातें ही रहीं। वो तो साॅफ्ट पोर्नोग्राफिक टाइप की चाहना लिए इसके पास आए थे। इसलिए ये उनके लिए निहायत ही नीरस साबित हुआ। वो तो इसके दूसरे पार्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद उसमें उन्हें ये नसीब हो। दूसरा भाग आया भी तो उसमें ये हसरत तो पूरी नहीं ही होगी। सनसनी फैलाकर सुर्खियाँ बटोरना मेरा मकसद नहीं है।
प्रश्न: आपका यात्रा 'वृत्तांत पंखों वाली लड़की की उड़ान' पाठकों को टर्की के नौ शहरों को दिखलाता है।टर्की से भारत का ऐतिहासिक नाता रहा है।
इस यात्रा के विषय में बताये? आपका कैसा अनुभव रहा?
उत्तर: बिल्कुल हमारे टर्की के साथ ऐतिहासिक संबंध लगभग हजार साल पुराने हैं। हालांकि शुरूआत अच्छी नहीं हुई थी। 986 में सुबुक्तगीन के द्वारा शाही वंश के राजा जयपाल पर आक्रमण के साथ हुई। इसके बाद इसके बेटे गजनवी के 1001 में और फिर लगातार सोलह और आक्रमण जिसमें 1025 का सोमनाथ का काफी प्रसिद्ध आक्रमण भी शामिल है, के साथ भारी लूटपाट। तत्पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा तुर्क साम्राज्य की स्थापना से लगाकर प्रथम विश्व युद्ध में टर्की के खिलाफ ब्रिटिश शासन ( जो हमारे भी शासक थे) का खड़ा होना और भारत को भी उसमें धकेलना, विरोध स्वरुप 1919 में मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में मुसलमानों द्वारा खिलाफत आंदोलन करना क्यूंकि मुगल काल से ही दुनिया के तमाम मुसलमान आटोमन तुर्कों को अपना खलीफा मानते थे। उनकी सहमति के बिना कोई कदम नहीं उठाते थे। बापू का उसी आधार पर 1920 में असहयोग आंदोलन करना। अभी फिलहाल कश्मीर मुद्दे पर टर्की का पाकिस्तान का साथ छोड़ हमारे पक्ष में खड़े होने तक एक समृद्ध इतिहास है।
एक लंबा साथ होने की वजह से ऐतिहासिक ही नहीं वरन सांस्कृतिक, भाषाई, कला, वास्तुकला, वेशभूषा, खानपान में भी भरपूर साम्यता है।
हमारी और उनकी भाषा में लगभग 9000 शब्द एक से हैं। चमचा, कैंची, चादर, छतरी, कुर्सी आप अपनी भाषा में वहाँ माँग सकते है। बहादुर को बहादुर, नौकर को नौकर और कुली को कुली कहकर पुकार सकते हैं।
मेरी यात्राएँ हमेशा भौगोलिक और ऐतिहासिक कोण के साथ उस जगह की मानवीय संदर्भों में नई आकृतियाँ खोजती हैं। तदुपरांत उन्हें मिट्टी सी कोमल भावभूमि पर साहित्य के गेरू से मांडने की तरह उकेरने की मेरी एक कोशिश भर रहती हैं।
इस यात्रा में भी ऐसे ही प्रेम पगे दाने-दुनके थे। जिन्हें मैंने एक पंछी की तरह उड़ान भरकर वहाँ जाकर उन्हें चुगा है। जो मैंनें ख़ुद अपनी आँखों से वहाँ जाकर देखा, महसूस किया, उसे बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना पूर्ववर्ती जानकारियों की एक भी लकीर का इस्तेमाल किये, पन्नों पर उतारा है। जानकारियाँ मोल मिल जाती हैं। जुड़ाव, जुड़ने पर ही मिलता है। ये यात्रा वृत्तांत उसका ही जीता जागता नमूना है।
ये यात्रा अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और उससे बढ़कर भौगोलिक समृद्धता के लिए मेरे लिए अविस्मरणीय बन पड़ी। यहाँ का एक शहर कैपेदोकिया अपनी भौगोलिक बनावट के लिए समूचे विश्व का नितांत निराला शहर है। हजारों सालों से प्रकृति के दुर्लभ कारनामों का इकलौता इतना व्यापक और सुघड़ नमूना। इसके आगोश में कुछ समय बिता कर बरसों पुरानी चाहत का पूरा होना किसी नेमत से कम नहीं था।
प्रश्न: आपका गद्य काव्यात्मक है, शिल्प प्रधान है। ऐसे में कथ्य और शिल्प के बीच के सामंजस्य को आप कैसे बरकरार रखती हैं? यह प्रश्न इसलिए भी क्योंकि कई बार रचनाकार शिल्प पर इतना ध्यान देते हैं (पर्पल प्रोज़) कि कथ्य गड़बड़ा जाता है, और पाठक शिल्प में ही उलझकर रह जाता है? आप इसे कैसे देखती हैं?
उत्तर: ये अब तक का सबसे उम्दा सवाल है। मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगी कि 'करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान'। लेकिन उससे भी पूर्व तो यह कि मैं मूलतः भावुक प्रवृत्ति और सौंदर्य बोध से ओत-प्रोत हृदय की मालकिन हूँ। भावनाएँ काव्य का स्थायी भाव है जैसे विचार गद्य के होते हैं। ऐसी अवस्था में जब मैं गद्य भी लिखूँ उसमें मूल स्वभावानुसार काव्यात्मकता का रिसकर चले आना कोई अचरज का मुद्दा नहीं। ठीक वैसे जैसे कविताओं में कई बार वैचारिक गंभीरता का ठोस भाव बलात पैठ जाता है। हर काम को ख़ूबसूरती से करना मेरा अंदाज है। इस हिसाब से मुझे इनमें तालमेल बिठाने हेतु कोई विशेष युक्ति नहीं अपनानी होती। ना ही सप्रयास ये करना पड़ता है। यह स्वभावत: अपने आप उपजता है। इतने अध्ययन के बाद भी अगर ये गुण मंजता नहीं तो इससे निरर्थक बात क्या तो होती।
दूसरा यह कि लेखन कार्य, वो लिख देना भर नहीं है जो हमें पता है। ये एक कला है। हर कला का अपना सौंदर्य होता है वो उसके शिल्प से ही निखरता है। ये आम बोलचाल नहीं है। बोल दी और बात ख़तम। लिखा हुआ हमेशा के लिए रह जाना है। उसे सुंदरतम रुप में ही जीवित रहना चाहिए। वरना कला तो अपने सादे रुप में भी उतनी ही अपील करती है। वैसे ही लेखन में भी है।
एक होता है कहना और एक होता है सौंदर्य बोध के साथ कहना। लेखन में शिल्प उसी सौंदर्य को बढ़ाता है।
'अति सर्वत्र वर्जयेत' की तर्ज़ पर यदि लिखते समय सादगीपूर्ण बात को भी 'पर्पल प्रोज़' के रुप में (अति आडंबर के साथ सजा-धजा कर) पेश किया जाये सिर्फ़ अपनी भाषाई पकड़, अपने समृद्ध शब्दकोष, खनकते मुहावरों, शब्दशक्तियों, अलंकारों, उपमाओं और बिंबों के रुप में स्वरचित ऊचाँई का ढ़िंढोरा पीटने के लिए। दूसरों को हतप्रभ करने के लिए, तो कथ्य निखरने की बजाय कृत्रिम रुप ले लेता है।वो लुभाता नहीं खिन्नता पैदा करता है।सहज रुप में आने पर ही कथ्य आकर्षण पैदा करता है।
कल्पना कीजिए एक नैसर्गिक सुंदरता से भरी रुपसी और दूजी गाढ़े मेकअप से लिपी पुती सुंदरी की। फ़र्क स्पष्ट नज़र आएगा।
ठीक ऐसे ही लेखन में शिल्प की घुंघराली घटाओं के बीच कथ्य का चाँद कहीं गुम होकर रह जाता है।
इसे ऐसे समझिये। दो भिन्न शैली के नृतक है।एक कथकली नृतक है, एक बैले नृतक है। दोनों ही शास्त्रीय नृत्य करते हैं। जिनमें भाव-भंगिमा और मुद्राओं पर जोर रहता है। इस आधार पर दोनों समान हैं, इसे लेखन का कथ्य मानिये। लेकिन कथकली में जितनी सजधज के साथ नृतक नृत्य करता है, वहीं बैले नृतक की वेशभूषा अत्यधिक सादगीपूर्ण होती है। ये शिल्प हुआ। बैले नृतक अगर कथकली की मानिंद भारी भरकम धजा में बैले करने लगे तो नृत्य को छोड़ उसका सारा ध्यान तो अपनी पोशाक को संभालने में लगा रहेगा। इसी तरह कथकली में आधा नृत्य तो वेशभूषा,मेकअप के सहारे दर्शाया जाता है, अगर वो उसे धारण किये बिना नृत्य करेगा तब तो उसकी कला निस्तेज ही रह जाएगी।
दोनों ही पहलुओं में देखने वाला ठगा सा रह जाएगा।
कहने का तात्पर्य ये कि विषय-वस्तु के हिसाब से कथ्य अलंकृत किये जायेंगें तो ख़ूबसूरत और लय ताल में बने रहेंगें।
अन्यथा उनका बेसुरा होकर हास्यास्पद बन जाना ही नियति होगी।
उम्मीद है मैं तथ्य को ठीक तरह सामने रख पाई।
प्रश्न: आप आजकल क्या लिख रहीं हैं? क्या अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के विषय में बतलाना चाहेंगीं?
उत्तर: एक किस्सों की कोठार लबालब भर कर उफनने पर उतारू है।
कुछ संस्मरण संदूक से बाहर निकलने को उतावले हो रहे हैं।
यात्रा वृत्तांत तो यादों के परकोटे से लटककर अपनी गरदन उचकाये इतनी निरीहता से मेरा मुँह ताकते रहते हैं कि मानो गुहार लगा रहे हों, कितनी जल्दी इस कैद से रिहाई देंगी हमें।
और एक हास्य-व्यंग्य का पिटारा है जो फूट पड़ने को मचल रहा है।
देखें कैसे रंग लाती है हिना? लग भी पाती है या नहीं? बाक़ी तो रब राखे।
प्रश्न: आजकल लाॅकडाउन चल रहा है। इस समय को आप कैसे देखती हैं? आप किस तरह समय बिता रहीं हैं?
उत्तर: बहुत अच्छी सीखों की अमानत मुट्ठी में बाँधे एक बेहद बेढंगा, खरखरा समय।
इस समय के दौरान कई इतनी अच्छाईयाँ उभर कर सामने आईं जिन्हें अपनी बदगुमानी में हम लगभग उन्हें बिसरा ही चुके थे।
और कई बुराइयाँ जिनके बारे में हम मुगालते में थे कि बुरे वक्त में तो वे भी शर्मसार होकर दम तोड़ देंगीं, पर उनका बेशर्मी से सीना तानकर खड़े रह जाना।
ये समय अपने अंदर झाँककर स्व-आकलन करने का है। हम किस तरह कुदरत पर कुंडली मारकर बैठे हुए थे।उसकी एक अकड़ाहट ने हमें हमारी सीमाएँ दिखा दी हैं। हम कितने कम संसाधनों में निर्वाह कर सकते हैं, पर उन्हें हपसे में भकोसते जा रहे हैं। रोबोट की तरह यंत्रवत काम करते-करते मशीन बनते जा रहे हैं। बिना किसी अहम लक्ष्य के भागते जा रहे हैं। इस भागमभाग में आपसी दूरियाँ बढ़ाते और अपनापन घटाते जा रहे हैं।
कुछ दोयम दर्जे के बेहया लोग अपना स्तर बनाये रखते हुए स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए है। भरपूर लूट-खसोट में भी।
इसी दौरान बहुतेरे अच्छे लोगों द्वारा निस्वार्थ सेवाएं भी की गई। खाली समय को रचनात्मक कार्यों से पाटा भी गया।
जो जैसा था उसने उसी हिसाब से इस समय को लिया अपनी पीढ़ी को विरासत में यादों के तौर पर देने के लिए। इससे ज़्यादा क्या कहा जाये?
नुकसान पारिवारिक सामाजिक आर्थिक तौर पर बहुत है, लेकिन अंतर्मन को जगाने का, मानसिक तौर पर मजबूत होने का ये माध्यम ज़रूर हो सकता है। आख़िरकार विपत्तियों में ही हम मजबूती से खड़े होते हैं।
सीखा तो बहुत कुछ पर बहुत बड़ी कीमत चुका कर। काश, हम बिना दबाव के संतुलन साधना सीख जाते तो ये दिन ना देखना पड़ते।
मैं तो लिखने-पढ़ने, चित्रकारी, बागबानी, कुकिंग करने जैसे शौकों से दो-दो हाथ कर रही हूँ। बाक़ी काम तो घर बैठे हो ही रहा है। घर में सबके संग हँसते, बोलते-बतियाते। योग और संगीत के सहारे हल्के होते हुए।
प्रश्न: प्रश्न तो कभी खत्म नहीं होते हैं लेकिन फिर भी बातचीत करते हुए काफी कुछ कहना पूछना छूट जाता है। इस बातचीत को विराम देने से पहले आखिर में ऐसा कुछ जो पूछने से रह गया हो और आप पाठकों से कहना चाहती हों?
उत्तर: इस पर तो इतना ही कहूँगी कि
मैं आदतन उतना ही कह पाती हूँ जितना पूछा जाता है।
फ़िर भी 'इस पार मैं' का आपने जिक्र नहीं किया जो मेरा काव्य संग्रह है, और मेरे दिल के काफ़ी करीब। कभी मौका मिले तो उसे भी समय दीजिये। उसमें एक अलहदा रुपाली मिलेगी।
निदा फ़ाज़ली कहते हैं ना--
हर आदमी में होते हैं दस बीस आदमी,
जिस को भी देखना हो कई बार देखना।
पाठक अब पहले ही ख़ूब जानकार होते हैं। एक अंगूठे तले सारा ज्ञान है। अब किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं।ना ही सुनने का वैसा हौसला ही रहा है अब।
सब आत्मनिर्भर हैं। सबके पास अमृत मंत्र भी है, अहम ब्रह्मास्मि।
कुछ कहते ही वो तपाक से कह उठेंगें, फ़ाज़ली साहेब के सुर में सुर मिलाकर, भले ही उन जितना गुना ना हो --
आँखों देखी कहने वाले, पहले भी कम-कम ही थे,
अब तो सब ही सुनी-सुनाई बातों को दोहराते हैं।
बहती गंगा हो तो उसमें हाथ ही नहीं धोने चाहिए, बल्कि डुबकी भी मार लेनी चाहिए, इस बात की मैं बड़ी कायल हूँ।
इस हिसाब से आपने जब बांसुरी हाथ में थमा ही दी है तो फूँक मार के कुछ तान तो अवश्य छेड़ूगीं ही --
'किसी इंसान से मिलना, ख़ुद आपका चलकर मिलना हो...
दूसरे के ज़रिये, नज़रिये से मिलना उसे कमतर करना है…!!'
अच्छा चलती हूँ दुआओं में याद रखना,
मेरे ज़िक्र का जुबाँ पे सुवाद रखना।
 |
| रुपाली नागर 'संझा' जी की पुस्तकें |
*****
तो यह थी रुपाली नागर 'संझा' जी की गयी हमारी बातचीत। उम्मीद है यह बातचीत आपको पसंद आयी होगी। साक्षात्कार के प्रति आपकी राय का हमें इन्तजार रहेगा।
© विकास नैनवाल 'अंजान'
FTC Disclosure: इस पोस्ट में एफिलिएट लिंक्स मौजूद हैं। अगर आप इन लिंक्स के माध्यम से खरीददारी करते हैं तो एक बुक जर्नल को उसके एवज में छोटा सा कमीशन मिलता है। आपको इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ये पैसा साइट के रखरखाव में काम आता है। This post may contain affiliate links. If you buy from these links Ek Book Journal receives a small percentage of your purchase as a commission. You are not charged extra for your purchase. This money is used in maintainence of the website.








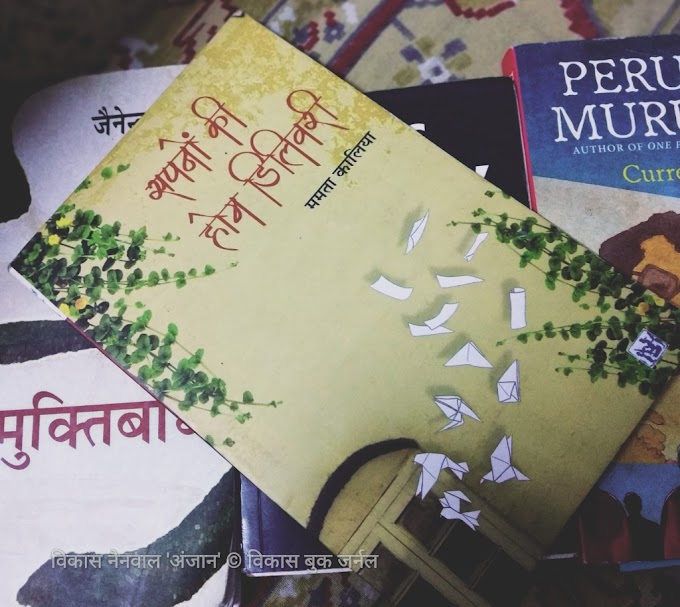

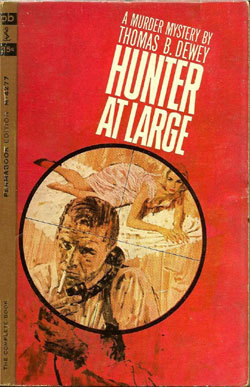

बहुत ही अच्छा साक्षात्कार प्रस्तुत किया है विकास जी आपने । मैंने रूपाली जी की पुस्तक 'पंखों वाली लड़की की उड़ान' पढ़ी है तथा उस पर रचयित्री को अपनी प्रतिक्रिया भी दी है । मैं 'संझा' (या 'सांझी') शब्द का आशय पहले से जानता था पर लेखिका ने इसे अपना उपनाम क्यों बनाया है, यह इस साक्षात्कार द्वारा ही पता चला । लेखिका के जीवन तथा व्यक्तित्व के विविध पहलुओं एवं साथ ही उनके विचारों से से अवगत करवाने के लिए बहुत-बहुत आभार आपका ।
ReplyDeleteजी, साक्षात्कार आपको पसंद आया यह जानकर अच्छा लगा। आगे भी मैं ऐसे रोचक बातचीत पेश करने की पूरी कोशिश रहेगी।
Deleteआज एक नया शब्द सीखा "लब्बोलुआब"
ReplyDeleteसाक्षात्कार अच्छा लगा मगर 2 जगह ऐतेहासिक तथ्य गलत थे।
सुबुक्तगीन तुर्की नस्ल का जरूर था मगर वह मध्य एशियाई था न की Turkey देश का। मध्य एशिया ही तुर्की नस्ल के मूल रहा है। यही से 11वी सदी मे तुर्की कबीले आज के turkey मे जा बसे थे और फिर तब उन्होंने एक तुर्की भाषी देश की निव रखी। आज का Turkey देश तुर्की उस्मानिया सल्तनत ने स्थापित किया था। मज़ेदार बात यह है की अनुवांशिक शोद्ध से पता चला है कि आज के turkey के अधिकांश लोग यूनानी लोगों के वंशज है। तुर्की मूल के लोग मुख्यतः शाशक वर्ग के ही रहे थे इसलिए वह कम थे।
दूसरी गलती है यह है कि मोहम्मद गौरी तुर्की नस्ल का नही था। वह एक फारसी-पठान था। उसका गुलाम सेनापति कुतुब उद दीन ऐबक एक तुर्की था। उसने भारत मे तुर्की सल्तनत की स्थापना की थी।
इस सल्तनत का Turkey से कोई लेना देना नही था सिवाय इसके की दोनो सल्तनतों के संस्थापक मध्य एशिया के तुर्की जाति के थे। मगर उस्मानिया सल्तनत का संस्थापक उस्मान प्रथम ओगुज़ कबीले का था जबकि कुतुब उद दीन ऐबक कबीले का।
जितना मुझे याद आ रहा है, मुग़लो और उस्मानिया सल्तनत के बीच ताल्लुख़ थे।
इससे भी पीछे जाना है आपको तो रोमन साम्राज्य तक जा सकते है। आज का Turkey रोम के अधीन रहा है और इस बात के सबूत है कि भारतीय व्यापारी रोमन साम्राज्य गए थे। शायद Turkey भी गए होंगे।
इससे भी पीछे जाना है तो फिर तुरकी पर Mittani नाम की जाति ने राज किया था। इनकी भाषा संस्कृत के करीब थी और इन्हें Indo-Aryan मूल का कहा गया है। वैज्ञानिको के अनुसार उत्तर भारतीय इसी मूल के है।
फिर प्रसिद्ध यूनानी ग्रंथ Illiad मे ज़िक्र है की ट्रॉय नरेश का भतीजा और इथियोपिया का राजा menmom ट्रॉय की रक्षा के लिए बड़ी सेना लेकर आया था। उस सेना मे भारतीय भी शामिल थे। और ट्रॉय आज के Turkey के पश्चिमी तट पर स्थित था।
देखिए इतिहास से जुड़ी बातें लिखते समय अच्छे से जांच कर लिया करे। लोग फिर गलत पढ़ेंगे और गलत सीखेंगे। यह एक इतिहास प्रेमी की आपसे इल्तिज़ा है। पाठक समझदार है आजके, मगर जिस विषय पर उन्हें ज्ञान नही, उसपर अगर कुछ भी लिख दिया जाए, तो वह आँख मूंदकर भरोसा कर लेते है।
साक्षात्कार आपको पसंद आया और आपने इतनी बारीकी से इसे पढ़ा यह जानकर अच्छा लगा। आपने सही कहा कि इतिहास की बातें दर्ज करते वक्त हमे ध्यान रखना चाहिए और यथासंभव स्रोतों का जिक्र कर देना चाहिए। लेखिका जी को यह करना चाहिए था। साक्षात्कार पर अपनी बहुमूल्य राय देने के लिए आभार।
Delete